RBSE Solutions for Class 11 Drawing Chapter 5 परवर्ती भित्ति-चित्रण परंपराएँ
Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 11 Drawing Chapter 5 परवर्ती भित्ति-चित्रण परंपराएँ Textbook Exercise Questions and Answers.
RBSE Class 11 Drawing Solutions Chapter 5 परवर्ती भित्ति-चित्रण परंपराएँ
RBSE Class 11 Drawing परवर्ती भित्ति-चित्रण परंपराएँ Textbook Questions and Answers
प्रश्न 1.
बादामी के गुफा भित्ति-चित्रों की क्या विशेषताएं हैं?
उत्तर:
बादामी की गुफाएँ छठी शताब्दी ईसवी के काल की हैं। इसकी गुफा संख्या 4 में सामने के मंडप की मेहराबदार छत पर भित्ति-चित्रों का सिर्फ एक ही अंश बचा है।
बादामी के भित्ति-चित्रों की विशेषताएँ
बादामी के गुफा भित्ति-चित्रों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
(1) भित्ति-चित्रों के विषय-बादामी की गुफा के भित्ति-चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसमें एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें कीर्तिवर्मन जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामन्तों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया है। दृश्य फलक के कोने की ओर इन्द्र और उसके परिकरों की आकृतियाँ हैं।
(2) शैलीगत विशेषताएं-शैली की दृष्टि से बादामी के चित्र दक्षिणं भारत में अजन्ता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परम्परा का विस्तार हैं। इन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- चित्रों की रेखाएं लयबद्ध हैं और धारा प्रवाह रूप लिये हुए हैं।
- चित्र का संयोजन चुस्त है। यह चुस्त संयोजन कला की कुशलता और परिपक्वता का सुंदर उदाहरण है जो ईसा की छठी शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती थी।
- राजा और रानी के मुखमण्डल रमणीय और लावण्यमय हैं, जो हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाते हैं।
- आकृतियों की आँखों के सॉकेट बड़े, आंखें आधी मिची और होंठ आगे निकले हुए दिखाए गए हैं।
- चेहरे के अलग-अलग हिस्सों की बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट हैं और सम्पूर्ण चेहरे को सुन्दरता प्रदान करती हैं। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के द्वारा सम्पूर्ण आकृति को भव्य बना दिया है।

प्रश्न 2.
विजयनगर के चित्रों पर निबंध लिखें।
उत्तर:
विजयनगर के भित्ति चित्र-तेरहवीं शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश ने दक्षिण में अपना आधिपत्य जमा लिया। यह राजवंश चौदहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक चला। इस राजवंश ने हम्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी विद्यमान हैं। यथा-
(1) विजयनगर भित्ति-चित्रों के स्थल-विजयनगर भित्ति-चित्रों के प्रमुख स्थल वहाँ के मंदिर हैं। यथा-
- त्रिची के पास (तिरुपराकुनरम, तमिलनाडु) में पाए गए चित्र, जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं।
- हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण-महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं।
- आधुनिक आंध्र प्रदेश में, हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं।

चित्र : दक्षिणामूर्ति, विजयनगर, लेपाक्षी
(2) विजयनगर भित्ति-चित्रों के विषय-
- हम्पी में, विरुपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर बने चित्र उस वंश के इतिहास की घटनाओं और रामायण व महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं।
- अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में एक चित्र में बुक्काराम के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है।
- साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है।
- लेपाक्षी मंदिर में वाराह को मारते हुए शिव और किरात अर्जुन को चित्रित किया गया है तथा पार्वती एवं अन्य नारी पात्रों का चित्रण किया गया है।
(3) विजयनगर भित्ति-चित्रों की कलात्मक विशेषताएं-विजयनगर भित्ति-चित्रों की कलात्मक विशेषताएं अग्रलिखित हैं-
- विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को दो आयामों में दिखाया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं।
- आकृतियों की आँखें बड़ी-बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है।
- रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई हैं और संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है।

प्रश्न 3.
केरल एवं तमिलनाडु भित्ति-चित्र परम्पराओं का वर्णन करें।
उत्तर:
केरल भित्ति-चित्र परम्परा केरल के चित्रकारों ने सोलहवीं से अठारहवीं सदी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। उन्होंने अपनी शैली में नायक (तमिलनाडु) और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच-समझकर अपना लिया था। यथा
(1) केरल भित्ति-चित्र स्थल-केरल के भित्ति-चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें ये तीन महल-(i) कोचि का डच महल, (ii) कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और (iii) पद्मनाभपुर महल। . जिन स्थलों पर केरल की भित्ति-चित्र परम्परा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है, वे हैं- पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पनायनरकावु, तिरुकोडिथानम्, त्रिपरयार का श्रीराम मंदिर और त्रिसूर का वडक्कुनाथन मंदिर।
(2) केरल के भित्ति-चित्रों के विषय-विषय की दृष्टि से केरल के चित्र शेष परम्पराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिन्दुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे।
ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपान्तर और मौखिक परम्पराओं को आधार बनाया था।

चित्र : वेणुगोपाल, श्रीराम मंदिर, त्रिपरियार

चित्र : गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए कृष्ण कृष्ण मंदिर, पुण्डरीकपुरम्
कलात्मक विशेषताएं-
केरल के कलाकारों ने कथककलि, कलम ऐझुथु (केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी) जैसी समकालीन परम्पराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली थी जिसमें कल्पनाशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था।
अधिकांश चित्र पूजागृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के भीतर चित्रित हुए हैं।
तमिलनाडु में भित्ति-चित्र परम्परा
उत्तर भारत की भित्ति-चित्र परम्परा पल्लव, पांड्य और चोलवंशी राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। तमिलनाडु की इस भित्ति-चित्र परम्परा को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है-
(1) पल्लवकालीन भित्ति-चित्र परम्परा-पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन प्रथम, जिसने सातवीं शताब्दी में शासन किया था, ने पनामलई, मंडगपट्ट और कांचीपुरम (तमिलनाडु) में मंदिरों का निर्माण कराया। मनामलई में देवी की मूर्ति लालित्यपूर्ण बनाई गई है।
कांचीपुरम मंदिर में सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राजसिंह के संरक्षण में बने थे।
इन भित्ति-चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं। रेखाओं में लयबद्धता है। अलंकरण की मात्रा पहले के चित्रों से अधिक है तथा धड़ को पहले की अपेक्षा अधिक लम्बा बनाया गया है।
(2) पांड्यकालीन चित्र परम्परा-पांड्य शासकों ने तिरमलईपुरम की गुफाओं और सित्तनवासल स्थित जैन गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया। सित्तनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रेकेट पर भित्तिचित्र विद्यमान हैं।
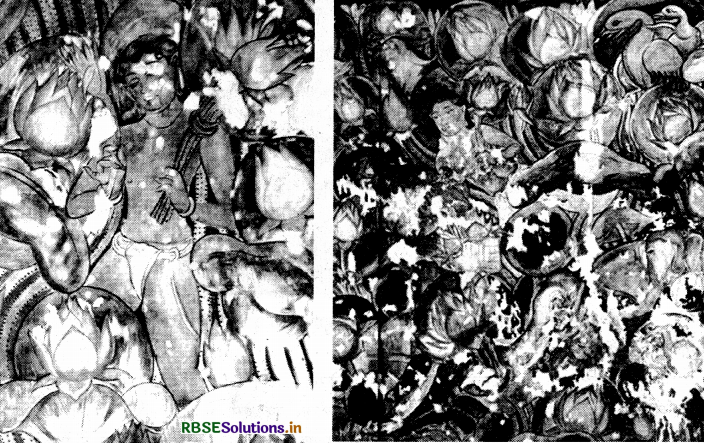
चित्र : सित्तनवासल, पूर्व पांड्य काल के चित्र, नवीं शताब्दी ईसवी
पांड्यकालीन भित्ति-चित्रों में बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियां हैं। इनकी बाहरी रेखाएं दृढ़ता से खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। शरीर का रंग पीला है और अंगों में लचक है। नर्तकियों के चेहरों पर भावों की झलक है, अनेक गतिमान अंग-प्रत्यंगों में लयबद्धता है। आंखें बड़ी-बड़ी हैं और कहीं-कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई हैं। आँखों की यह विशेषता दक्षिण भारत के परवर्ती काल के अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती है।
पांड्यकालीन चित्रों की उपर्युक्त सभी विशेषताएँ कलाकार की सर्जनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता की द्योतक हैं।

चित्र : देवी, सातवीं शताब्दी ईसवी, पनामलई
(3) चोलकालीन भित्ति-चित्र-चोल नरेशों ने 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक शासन किया। देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजाने-सँवारने की परम्परा चोल नरेशों के शासन काल में भी जारी रही।
11वीं शताब्दी में, जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुँचे तो चोल कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्तम नमूने सामने आए। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम् और दारासुरम् के मंदिर क्रमशः राजराज चोल, उसके पुत्र राजेन्द्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासन काल में बने।
वैसे तो नर्तनमलई में चोलकालीन चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन चोलकालीन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भित्तिचित्र बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में पाए जाते हैं। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों को दर्शाया गया है। जैसे-कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राजराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि को चित्रित किया गया है।
इन चित्रों में लहरियेदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह, आकृतियों के हाव-भाव और अंग-प्रत्यंगों की लचक देखने को मिलती है।
